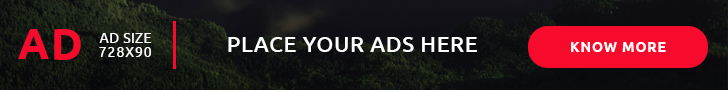क्या बहिष्कार फ़ेसबुक को नुक़सान पहुंचा सकता है? इसका जवाब 'हां' है।
18वीं शताब्दी में हुए 'उन्मूलनवादी आंदोलन' (एबोलिशनिस्ट मूवमेंट) ने ब्रिटेन के लोगों को ग़ुलामों की बनाई हुई वस्तुओं को ख़रीदने से रोका।
इस आंदोलन का बड़ा असर हुआ। लगभग तीन लाख लोगों ने चीनी ख़रीदनी बंद कर दी, जिससे ग़ुलामी प्रथा को ख़त्म किए जाने का दबाव बढ़ा।
'स्टॉप हेट फ़ॉर प्रॉफ़िट' वो ताज़ा अभियान है जिसमें 'बहिष्कार' को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मुहिम का दावा है कि फ़ेसबुक अपने प्लेटफ़ॉर्म पर नफ़रत से भरी और नस्लवादी सामग्री (कॉन्टेंट) हटाने की पर्याप्त कोशिश नहीं करता।
'स्टॉप हेट फ़ॉर प्रॉफ़िट' मुहिम ने कई बड़ी कंपनियों को फ़ेसबुक और कुछ अन्य सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म्स से अपने विज्ञापन हटाने के लिए राज़ी कर लिया है।
फ़ेसबुक से अपने विज्ञापन हटाने वालों में कोका-कोला, यूनीलीवर और स्टारबक्स के बाद अब फ़ोर्ड, एडिडास और एचपी जैसी नामी कंपनियां भी शामिल हो गई हैं।
समाचार वेबसाइट 'एक्सियस' के अनुसार माइक्रोसॉफ़्ट ने भी फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर मई में ही विज्ञापन देना बंद कर दिया था। माइक्रोसॉफ़्ट ने अज्ञात 'अनुचित सामग्री' की वजह से फ़ेसबुक पर विज्ञापन देने बंद किए हैं।
इस बीच रेडिट और ट्विच जैसे अन्य ऑनलाइन प्लंटफ़ॉर्म्स ने भी अपने-अपने स्तर पर नफ़रत-विरोधी क़दम उठाए हैं और फ़ेसबुक पर दबाव बढ़ा दिया है।
तो क्या इस तरह के बहिष्कार से फ़ेसबुक को भारी नुक़सान हो सकता है?
इस सवाल का छोटा सा जवाब है - हां। क्योंकि फ़ेसबुक के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापनों से ही आता है।
अवीवा इन्वेस्टर्स के डेविड कमिंग ने बीबीसी से कहा कि फ़ेसबुक से लोगों का भरोसा उठ गया है और यूज़र्स को फ़ेसबुक के रवैये में नैतिक मूल्यों की कमी नज़र आई है। डेविम कमिंग का मानना है कि ये धारणाएं फ़ेसबुक के कारोबार को बुरी तरह नुक़सान पहुंचा सकती हैं।
शुक्रवार को फ़ेसबुक के शेयर की कीमतों में आठ फ़ीसदी गिरावट दर्ज की गई थी। नतीजन, कंपनी के सीईओ मार्क ज़करबर्ग को कम से कम साढ़े पांच खरब रुपयों का नुक़सान हुआ।
लेकिन क्या ये नुक़सान और बड़ा हो सकता है? क्या इससे आने वाले दिनों में फ़ेसबुक के अस्तित्व को ख़तरा पैदा हो सकता है? इन सवालों के स्पष्ट जवाब मिलने अभी बाकी हैं।
पहली बात तो ये है कि फ़ेसबुक बहिष्कार का सामना करने वाली पहली सोशल मीडिया कंपनी नहीं है।
साल 2017 में कई बड़े ब्रैंड्स ने ऐलान किया कि वो यूट्यूब पर विज्ञापन नहीं देंगे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक ख़ास ब्रैंड का विज्ञापन किसी नस्लभेदी और होमोफ़ोबिक (समलैंगिकता के प्रति नफ़रत भरा) वीडियो के बाद दिखाया गया था।
इस ब्रैंड के बहिष्कार को अब लगभग पूरी तरह भुला दिया गया है। यूट्यूब ने अपनी विज्ञापन नीतियों में बदलाव किया और अब यूट्यूब की पेरेंट कंपनी गूगल भी इस सम्बन्ध में ठीक काम कर रही है।
हो सकता है कि इस बहिष्कार का फ़ेसबुक को बहुत ज़्यादा नुक़सान न हो। इसके कुछ और कारण भी हैं।
पहली बात तो ये कि कई कंपनियों ने सिर्फ़ जुलाई महीने के लिए फ़ेसबुक का बहिष्कार करने की बात कही है। दूसरी बात ये कि फ़ेसबुक के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा छोटे और मध्यम कंपनियों के विज्ञापन से भी आता है।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सबसे ज़्यादा ख़र्च करने वाले 100 ब्रैंड्स से फ़ेसबुक को तकरीबन तीन खरब रुपये की कमाई हुई थी और यह विज्ञापन से होने वाली कुल कमाई का महज़ छह फ़ीसदी था।
एडवर्टाइज़िंग एजेंसी डिजिटल ह्विस्की के प्रमुख मैट मॉरिसन ने बीबीसी को बताया कि बहुत-सी छोटी कंपनियों के लिए 'विज्ञापन न देना संभव नहीं है।'
मॉरिसन कहते हैं, "जो कंपनियां टीवी पर विज्ञापन के लिए भारी-भरकम राशि नहीं चुका सकतीं, उनके लिए फ़ेसबुक एक ज़रूरी माध्यम है। कारोबार तभी सफल हो सकता है जब कंपनियां अपने संभावित ग्राहकों तक पहुंच पाएं। इसलिए वो विज्ञापन देना जारी रखेंगी।''
इसके अलावा, फ़ेसबुक का ढांचा ऐसा है कि ये मार्क ज़करबर्ग को किसी भी तरह के बदलाव करने की ताक़त देता है। अगर वो कोई नीति बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ़ उनके विचारों को बदला जाना ज़रूरी है। अगर ज़करबर्ग कार्रवाई न करना चाहें तो नहीं करेंगे।
हालांकि पिछले कुछ दिनों में मार्क ज़करबर्ग ने बदलाव के संकेत दिए हैं। फ़ेसबुक ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वो नफ़रत भरे कमेंट्स को टैग करना शुरू करेगा।
दूसरी तरफ़, बाकी कंपनियां ख़ुद से अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं।
सोमवार को सोशल न्यूज़ वेबसाइट रेडिट ने ऐलान किया कि वो 'द डोनाल्ड ट्रंप फ़ोरम' नाम के एक समूह पर प्रतिबंध लगा रहा है। इस समूह के सदस्यों पर नफ़रत और धमकी भरे कमेंट करने का आरोप है। ये समूह सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं जुड़ा था लेकिन इसके सदस्य उनके समर्थन वाले मीम्स शेयर करते थे।
इसके अलावा ऐमेज़न के स्वामित्व वाले वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म ट्विच ने भी 'ट्रंप कैंपेन' द्वारा चलाए जाने वाले एक अकाउंट पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी है। ट्विच ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की रैलियों के दो वीडियो में कही गई बातें नफ़रत को बढ़ावा देने वाली थीं।
इसमें से एक वीडियो साल 2015 (ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले) का था। इस वीडियो में ट्रंप ने कहा था कि मेक्सिको बलात्कारियों को अमरीका में भेज रहा है।
ट्विच ने अपने बयान में कहा, "अगर किसी राजनीतिक टिप्पणी या ख़बर में भी नफ़रत भरी भावना है तो हम उसे अपवाद नहीं मानते। हम उसे रोकते हैं।''
ये साल सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए चुनौती भरा होने वाला है और फ़ेसबुक भी इन चुनौतियों के दायरे से बाहर नहीं है। हालांकि कंपनियां हमेशा अपनी बैलेंस शीट को ध्यान में रखकर फ़ैसले लेती हैं। इसलिए अगर ये बहिष्कार लंबा खिंचता है और ज़्यादा कंपनियां इसमें शामिल हो जाती हैं तो ये साल फ़ेसबुक के लिए काफ़ी कुछ बदल देगा।