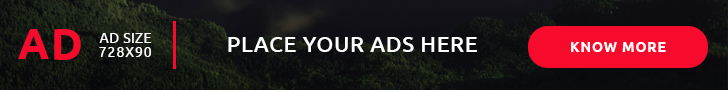चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ पहुंचे। 19 साल बाद यह पहला मौक़ा है जब कोई चीनी राष्ट्रपति म्यांमार के दौरे पर है।
वैसे तो जिनपिंग दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों की 70वीं वर्षगांठ पर म्यांमार आए हैं मगर इस यात्रा के दौरान वह म्यांमार की शीर्ष नेता आंग सान सू ची के साथ मिलकर चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे के तहत कई परियोजनाओं को शुरू करेंगे।
शी जिनपिंग के दौरे से पहले चीन के उप विदेश मंत्री लाउ शाहुई ने पत्रकारों से कहा था कि राष्ट्रपति की इस यात्रा का मक़सद दोनों देशों के रिश्तों को मज़बूत करना और बेल्ट एंड रोड अभियान के तहत आपसी सहयोग बढ़ाना है।
उन्होंने कहा था कि इस दौरे का तीसरा लक्ष्य है 'चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे को मूर्त रूप देना।' चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड अभियान का ही अंग है।
चीन के इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भारत शक की निगाहों से देखता रहा है क्योंकि उसका मानना है कि इस अभियान के तहत चीन दक्षिण एशियाई देशों में अपना प्रभाव और पहुंच बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है।
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फ़ॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफ़ेसर रितु अग्रवाल कहती हैं कि चीन और म्यांमार के बीच अच्छे संबंधों की शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी।
वह बताती हैं, "चीन और म्यांमार काफ़ी क़रीबी कारोबारी सहयोगी रहे हैं। चीन के युन्नात प्रांत में म्यामांर की सीमा के साथ 2010 से लेकर अब तक कई सारे बॉर्डर इकनॉमिक ज़ोन बनाए गए हैं और आर्थिक आधार पर म्यांमार को चीन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि यहां से ऑयल और गैस पाइपलाइन बिछाने की भी बात थी।''
रितु अग्रवाल बताती हैं कि युन्नान की प्रांतीय सरकार ने अपने स्तर पर म्यामांर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की थी। यह सिलसिला 80 के दशक से शुरू हुआ था। हालांकि, बीच में कई उतार-चढ़ाव आए। मगर अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से इस कोशिश को जारी रखा जा रहा है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेश नीति का अहम हिस्सा माना जाता है। इसे सिल्क रोड इकनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड भी कहा जाता है। जिनपिंग ने 2013 में इसे शुरू किया था।
बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत चीन का इरादा कम से कम 70 देशों के माध्यम से सड़कों, रेल की पटरियों और समुद्री जहाज़ों के रास्तों का जाल सा बिछाकर चीन को मध्य एशिया, मध्य पूर्व और रूस होते हुए यूरोप से जोड़ने का है। चीन यह सब ट्रेड और निवेश के माध्यम से करना चाहता है।
चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भौगोलिक रूप से म्यांमार काफ़ी अहम है। म्यांमार ऐसी जगह पर स्थित है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच है। यह चारों ओर से ज़मीन से घिरे चीन के युन्नान प्रांत और हिंद महासागर के बीच पड़ता है इसलिए चीन-म्यांमार इकनॉमिक कॉरिडोर की चीन के लिए बहुत अहमियत है।
रितु अग्रवाल बताती हैं, "चीन काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा है कि कैसे हिंद महासागर तक पहुंचे। शी जिनपिंग की ताज़ा यात्रा चीन की समुद्री शक्ति को बढ़ाने की कोशिश में है क्योंकि चीन का समुद्री शक्ति बढ़ाना शी जिनपिंग की प्राथमिकताओं में है। इसलिए वह पोर्ट बनाने, रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। वह इनके माध्यम से कनेक्टिविटी चाहते हैं।''
अप्रैल 2019 में हुए चीन के दूसरे बेल्ट एंड रोड फ़ोरम (बीआरएफ) में म्यांमार की नेता आंग सान सू ची ने 'चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे' (सीएमईसी) के तहत सहयोग बढ़ाने के लिए चीन के साथ तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे।
चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा अंग्रेज़ी के Y अक्षर के आकार का एक कॉरिडोर है। इसके तहत चीन विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंचकर म्यांमार के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहता है।
2019 से 2030 तक चलने वाले इस आर्थिक सहयोग के तहत दोनों देशों की सरकारों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन, कृषि, परिवहन, वित्त, मानव संसाधन विकास, शोध, तकनीक और दूरसंचार जैसे कई क्षेत्रों में कई सारी परियोजनाओं को लेकर सहयोग करने पर सहमति बनी थी।
इसके तहत चीन के युन्नान प्रांत की राजधानी कुनमिंग से म्यांमार के दो मुख्य आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए लगभग 1700 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाना है।
कुनमिंग से आगे बढ़ने वाले इस प्रॉजेक्ट को पहले मध्य म्यांमार के मंडालय से हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ा जाएगा। फिर यहां से इसे पूर्व में यंगॉन और पश्चिम में क्यॉकप्यू स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन से जोड़ा जाएगा। चीन क्यॉकप्यू में पोर्ट भी बनाएगा।
इस अभियान के तहत म्यांमार की सरकार ने शान और कचिन राज्यों में तीन बॉर्डर इकनॉमिक कोऑपरेशन ज़ोन बनाने पर सहमति जताई थी।
चीन का कहना है कि सीएमईसी से म्यांमार के दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में सीधे चीनी सामान पहुंच सकेगा और चीन के उद्योग भी सस्ते श्रम की तलाश में ख़ुद को यहां शिफ़्ट कर सकते हैं। यह दावा किया जाता रहा है कि म्यांमार इस परियोजना के कारण चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के बीच कारोबार का केंद्र बन जाएगा।
लेकिन चीन और म्यांमार के बीच युन्नान के साथ लगती सीमा पर कई तरह की पहलों के चलते बने संबंध पूरी तरह आर्थिक संबंध ही हैं, ऐसा भी नहीं है। रितु अग्रवाल कहती हैं कि इस तरह के आर्थिक अभियानों के पीछे कहीं न कहीं सुरक्षा का एजेंडा रहता है।
संभवत: भारत की चिंताएं भी इसी से जुड़ी हैं।
भारत के लिहाज़ से देखें तो चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे को कुछ विश्लेषक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की तरह मान रहे हैं जो चीन के पश्चिमी शिनज़ियांग प्रांत को कराची और फिर अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। वैसे ही चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा चीन को बंगाल की खाड़ी की ओर से समंदर से जोड़ता है।
इसके अलावा, पिछले साल शी जिनपिंग ने नेपाल यात्रा के दौरान चीन-नेपाल आर्थिक गलियारे की शुरुआत की थी। इसके तहत चीन का इरादा तिब्बत को नेपाल से जोड़ना है। चीन नेपाल कॉरिडोर, चीन-पाकिस्तान और चीन-म्यांमार गलियारों के बीच में पड़ता है।
इस तरह तीनों गलियारे का चीन को कारोबारी स्तर पर लाभ होगा मगर भारत की चिंताएं सुरक्षा को लेकर भी रहती हैं। रितु अग्रवाल कहती हैं कि भारत को पहले से ही इस बात की चिंता है कि कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ सुरक्षा को लेकर भी ख़तरा बढ़ सकता है।
वह कहती हैं, "चीन जो भी कनेक्टिविटी करता है, उसमें वह इकनॉमिक कॉरिडोर की बात करता है मगर उसके पीछे भी दूसरों की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने जैसी रणनीतियां रहती हैं। यह चीन का तरीक़ा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि दक्षिण एशिया में उसके पड़ोसी अगर चीन के नियंत्रण में आ गए तो उसे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने में दिक्कत होगी।''
चीन ने भारत को भी अपने इस अभियान में शामिल करने की कोशिशें की हैं मगर भारत ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि, चीन मामलों के जानकार अतुल भारद्वाज मानते हैं कि चीन की पहुंच म्यांमार कॉरिडोर के माध्यम से हिंद महासागर तक हो जाने से भारत को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बीबीसी से कहा, "भारत हमेशा से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने के समर्थन में रहा है इसलिए उसे किस बात का डर होगा? बल्कि उसे तो अपने आसपास शुरू होने वाली नई परियोजनाओं में आर्थिक अवसरों की तलाश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीन उन हिस्सों को जोड़ रहा है जो अछूते रहे हैं। वह सिर्फ़ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वैकल्पिक रास्ते मुहैया करवा रहा है।''
भारत भी अपनी विदेश नीति में 'लुक ईस्ट पॉलिसी' की बात करता रहा है। इसके तहत यह कहा जाता रहा कि भारत के संबंध म्यांमार के साथ अच्छे होने चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार पूर्वोत्तर राज्यों के जरिये 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी का ज़िक्र कर चुके हैं।
अगर भारत दक्षिण पूर्वी देशों के साथ आर्थिक और कारोबारी सहयोग बढ़ाना चाहता है तो उसका रास्ता म्यांमार से होकर ही जाता है। मगर भारत की लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट के नारों वाली नीतियों के बावजूद म्यांमार में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ा है।
रितु अग्रवाल कहती हैं कि भारत का म्यांमार के साथ ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक रिश्ता रहा है, इसलिए चीन के प्रयासों को लेकर चिंता करने की जगह अपनी ओर से गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए।
वह कहती हैं, "ऐतिहासिक रूप से भारत के उत्तर पूर्व और कलकत्ता के म्यांमार से अच्छे रिश्ते थे, दोनों देशों में सीधे व्यापारिक संबंध थे और यातायात भी होता था। यह देखा जाना चाहिए कि कैसे इसे फिर से जीवंत किया जा सकता है।''
"भारत अपनी ओर से पहल करके म्यांमार के साथ कोई मिशन शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम उठा सकता है। भारत दक्षिण एशिया में शुरू से बड़ी शक्ति रहा है। ऐसे में चिंतित होने की जगह उसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मज़बूत करने की रणनीति बनानी चाहिए। उसे देखना होगा कि क्या पहल करके वह चीन के प्रभाव को सीमित कर सकता है।''
भारत पर तीन दिशाओं से बेल्ट एंड रोड अभियान के तहत चीन की पहुंच होने को लेकर रितु अग्रवाल कहती हैं, "भारत की चिंताएं तो हैं मगर अहम बात यह है कि उसकी आगे की रणनीति क्या होगी? कैसे पड़ोसियों के साथ ट्रेड डील की जा सकती है, कैसे व्यापारिक रिश्ते मज़बूत किए जा सकते हैं। कोई प्रभावी नीति होनी चाहिए।''
शी जिनपिंग पर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सफल बनाने का दबाव बना हुआ है। बहुत सारे देशों ने उनकी पहल को लेकर इच्छा तो जताई थी मगर पायलट प्रॉजेक्ट्स के नतीजे चीन की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे हैं। म्यांमार में भी विरोध के स्वर उठते रहे हैं।
ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि भारत को अपनी ओर से सकारात्मक पहल करके पड़ोसियों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करनी चाहिए और इस संबंध में उसे कोई स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत की मोदी सरकार अपनी आर्थिक मंदी के कारण चीन को रोकने में सफल होगी?