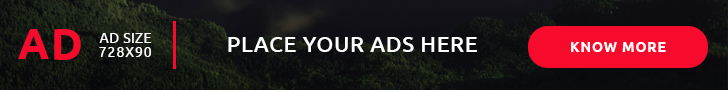भारत ने 7 सितंबर 2020 को ओडिशा के तट से हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट तकनीक का परीक्षण किया जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है।
भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने हाइपरसोनिक तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
भारत में तैयार किए गए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोनस्ट्रेटर व्हीकल (एचएसटीडीवी) का लंबी दूरी की मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
7 सितंबर 2020 को उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से इसे सफलतापूर्वक भेजा गया।
डीआरडीओ ने इस मौक़े पर कहा कि इस मिशन के ज़रिए डीआरडीओ ने जटिल तकनीक को लेकर अपनी क्षमता दिखाई है और ये नेक्सटजेन (उन्नत) हाइपरसोनिक व्हीकल बनाने के लिए एक नींव की तरह काम करेगा।
डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का इस्तेमाल कर एक मिसाइल दाग़ा जिसने वायुमंडल में जाकर माक-6 तक की स्पीड हासिल कर ली।
डीआरडीओ ने इसे रक्षा तकनीक के मामले में बड़ी उपलब्धि बताया है। लेकिन ये तकनीक क्या है? भारत के रक्षातंत्र में ये कैसे मददग़ार होगा?
हाइपरसोनिक स्पीड क्या है?
ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड से छोड़ा जा सकता है।
पॉपुलर मेकैनिक्स के अनुसार विज्ञान की भाषा में हाइपरसोनिक को 'सुपरसोनिक ऑन स्टेरायड्स' कहा जाता है यानी तेज़ गति से भी अधिक तेज़ गति।
सुपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की गति से तेज़ (माक-1) और हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब है सुपरसोनिक से भी कम से कम पांच गुना अधिक की गति। इसकी गति को माक-5 कहते हैं, यानी आवाज़ की गति से पांच गुना ज़्यादा की स्पीड।
हाइपरसोनिक स्पीड वो गति होती है जहां तेज़ी से जा रही वस्तु के आसपास की हवा में मौजूद अणु के मॉलिक्यूल भी टूट कर बिखरने लगते हैं।
डीआरडीओ का कहना है कि जिस यान का प्रक्षेपण हुआ है वो पहले आसमान में 30 किलोमीटर ऊपर तक गया, और फिर उसने माक-6 की स्पीड पकड़ी।
स्क्रैमजेट तकनीक क्या है?
भारत के वैज्ञानिक गौहर रज़ा बताते हैं ये समझने से पहले हमें न्यूटन के सिद्धातों में से एक अहम सिद्धांत के बारे में पहले जानना होगा।
न्यूटन की गति के सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत कहता है कि 'प्रत्येक क्रिया के बदले हमेशा और विपरीत प्रतिक्रिया होती है'। इसका मतलब ये कि रॉकेट के भीतर जब ईंधन जलाया जाता है और उसकी गैस बाहर निकलती तो इसकी प्रतिक्रिया स्परूप रॉकेट (व्हीकल) को एक तेज धक्का लगता है जो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। इसी को जेट प्रोपल्शन कहते हैं।
शुरूआती दौर में जो जेट बने उनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला कर बने ईंधन को जलाया जाता है और इसके लिए रॉकेट के भीतर ईंधन रखना होता है।
1960 के दशक में एक ऐसी तकनीक के बारे में सोचा गया जिसमें ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन रॉकेट में न रख कर वायुमंडल से लिया जा सके। इस तकनीक को रैमजेट तकनीक कहा गया।
1991 तक पहुंचते-पहुंचते तत्कालीन सोवियत संघ ने साबित किया कि अधिक स्पीड पर ऑक्सीजन बाहर से न लेकर सोनिक स्पीड तक पहुंचा जा सकता है लेकिन सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचना मश्किल होता है, इसके लिए हमें स्क्रैमजेट तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी।
इस नई तकनीक में रॉकेट वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और अपनी स्पीड बढ़ाता है। इसका लाभ ये होता है कि रॉकेट में दोगुना ईंधन भरने की ज़रूरत नहीं रह जाती।
लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल केवल वायुमंडल के भीतर हो सकता है। अगर रॉकेट वायुमंडल से बार निकल जाए तो ये तकनीक नाकाम होने का ख़तरा होता है। ये तकनीक सबसे पहले सोवियत संघ ने 1991 में इस्तेमाल कर माक की स्पीड हासिल करने का दावा किया।
सोवियत संघ के परीक्षण के कई सालों बाद अमरीका ने इस तकनीक का सफल परीक्षण किया जिसके बाद चीन ने इसका सफल परीक्षण किया है।
ऐसे में भारत स्क्रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।
स्क्रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल
इस तकनीक का इस्तेमाल रॉकेट में और मिसाइल में किया जा सकता है। किसी भी मिसाइल में तीन बातें अहम होती हैं -
स्पीड - मिसाइल कितनी स्पीड तक पहुंच पाती है? स्क्रैमजेट तकनीक मिसाइल को कितना मज़बूत धक्का देकर आगे बढ़ा सकती है? अगर धक्का इतना मज़बूत हुआ कि वो मिसाइल को वायुमंडल से बाहर लेकर चला गया तो वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो बेकार हो जाएगी।
ईंधन जलने का वक्त - ईंधन कितनी देर तक जलता है? वो मिसाइल की स्पीड को कितनी देर तक बरकरार रख पा रहा है? मोटै तौर पर कहा जाए तो ईंधन कितनी देर तक जलता रह सकता है?
लक्ष्य तक मार करने की क्षमता - ये तकनीक मिसाइल या रॉकेट को अपने लक्ष्य तक ठीक से पहुंचा पा रहा है या नहीं क्योंकि तेज़ गति के साथ लक्ष्य पर सटीक मार करना मुश्किल हो सकता है। इतनी स्पीड पर ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। जब मिसाइल व्हीकल से अलग होता है तब वो ठीक से अलग हो और सही निशाने पर जाए ये बेहद ज़रूरी है।
गौहर रज़ा कहते हैं कि इस तकनीक से भारत को दो बड़े फायदे होंगे। पहला तो ये कि रक्षा क्षेत्र में इसका बहुत योगदान होगा क्योंकि मिसाइल के लक्ष्य तक पहुंचने का समय कम हो जाएगा।
दूसरा ये कि रॉकेट भेजने के वक्त ईंधन बचाना भी अब संभव हो सकेगा, ख़ास कर तब तक जब तक रॉकेट वायुमंडल में है। इससे व्हीकल का वज़न कम होगा।