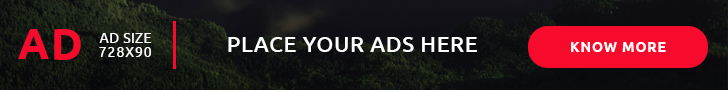रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ख़ुद ही मंगलवार को कोरोना वायरस की दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने की घोषणा की थी। रूस ने इस वैक्सीन का नाम स्पूतनिक 5 रखा है।
जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है ऐसे में वैक्सीन बनने को लेकर जश्न मनाया जाना चाहिए था लेकिन इतनी उदासीनता क्यों है?
ऐसा इसलिए है कि वैक्सीन बनाने की दौड़ में दुनिया के कई देश शामिल थे। ऐसे में रूस का बाज़ी मार जाना कई देशों को नागवार गुजरा। ऐसा इसलिए है कि कई देश कोरोना महामारी को भी अवसर के रूप के देखते है। उनके लिए कोरोना महामारी व्यापार का बड़ा अवसर लेकर आया है।
रूस के द्वारा सबसे पहले वैक्सीन बनाने की घोषणा से इन देशों को इस महामारी से खरबों डॉलर कमाने के मंसूबों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ़ रूस अपनी वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। जो इन देशों के जले पर नमक छिड़कने के समान है। अब वैक्सीन के दौड़ में पिछड़ने के बाद ये देश रूस के वैक्सीन में तरह-तरह का कमी निकालने की कोशिश करेंगे।
भारत में कोरोना के कारण हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या के हिसाब से भारत चौथे नंबर पर पहुँच गया है। तब भी रूस की वैक्सीन को लेकर कोई उत्साह नहीं है। भारत में गुरुवार तक कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 24,61,190 तक पहुंच गया है। भारत में एक दिन में 64,553 नए मामले सामने आए और 1,007 लोगों की मौत हो गई।
अब तक कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या 48,040 हो गई है। देश में कोरोना वायरस के 6,61,595 एक्टिव मामले मौजूद हैं और 17,51,555 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं।
राज्यों के स्तर पर देखें तो सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। यहां अब तक 56,01,26 मामले आ चुके हैं। सबसे कम 649 मामले मिजोरम में हैं।
भारत को समझना होगा कि या तो वह खुद जल्द से जल्द अपना वैक्सीन बना ले। या उसे जहाँ से भी वैक्सीन मिले, उसे खरीद कर पूरे देश में लोगों को वैक्सीन दे। भारत को यह समझना होगा कि उसे वैक्सीन कोई भी देश मुफ्त में तो देगा नहीं, फिर किसी देश का इंतजार क्यों? भारत को सिर्फ अपने नागरिकों के बारे में सोचना होगा, अन्यथा जिस तेजी से भारत में कोरोना महामारी फ़ैल रही है, उससे भारत को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
भारत की तुलना में ब्राज़ील कोरोना वायरस की महामारी में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। यहां एक लाख से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद ब्राज़ील रूसी वैक्सीन को लेकर संदेहग्रस्त और उदासीन है। ब्राज़ील ने कहा है कि रूसी वैक्सीन ख़रीदने से पहले उसे और सूचना चाहिए।
ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को कहा कि रूसी वैक्सीन को लेकर वो अभी और बात करेंगे। कोरोना वायरस की चपेट में सबसे बुरी तरह से आने वालों देशों में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है।
ब्राज़ील अपने यहां कई वैक्सीन का ट्रायल भी करवा रहा है। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री एडुअर्डो पाज़ेउलो ने कहा कि रूसी वैक्सीन अभी शुरुआती चरण में है।
उन्होंने कहा, ''अभी तो यह वैक्सीन आई ही है। इसके बारे में मेरे पास ऐसी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है जिसके आधार पर कुछ कह सकूं। हमलोग इसके डेटा की निगरानी नहीं कर रहे हैं। अभी इसके बारे में बहुत कुछ बात करने की ज़रूरत है।''
सीएनएन के अनुसार रूस ने अमरीका को कोविड 19 से निपटने के लिए अपनी वैक्सीन देने का प्रस्ताव रखा था लेकिन अमरीका ने ऐसी कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया है।
सीएनएन से एक रूसी अधिकारी ने कहा, ''दोनों देशों में भरोसे की कमी है ऐसे में टेक्नोलॉजी, वैक्सीन, टेस्टिंग और इलाज में सहयोग शायद ही संभव है।''
गुरुवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी काइली मैकनानी ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप को रूस की वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई है। काइली ने कहा कि अमरीका में वैक्सीन का काम चल रहा है और सब कुछ सकारात्मक है।
उन्होंने कहा कि अमरीका की वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है और बहुत ही मानक स्तर का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस की वैक्सीन के बारे में कहा है कि उसे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है इसलिए वो कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता।
रूस की वैक्सीन पर भारत ने अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है।