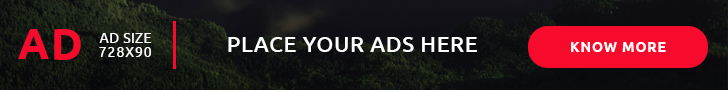सीरिया में अमरीका की सैन्य नीति में बदलाव से भारी उठापटक की बात कही जा रही है। अमरीका ने उत्तर-पूर्वी सीरिया से अपने सैनिकों को बुलाने का फ़ैसला किया है।
हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह फ़ैसला पेंटागन के अधिकारियों की सोच के उलट है, जो चाहते थे कि उत्तर-पूर्वी सीरिया में अमरीकी सैनिकों की छोटी संख्या मौजूद रहे। पेंटागन चाहता है कि उत्तर-पूर्वी सीरिया में अमरीका का इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ अभियान ख़त्म नहीं हो।
कहा जा रहा है कि अमरीका के इस क़दम से सीरिया में रूस और ईरान का प्रभाव बढ़ेगा। इस इलाक़े में अमरीका कुर्दों के साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ अभियान चलाता रहा है। दूसरी तरफ़ तुर्की कुर्द बलों को आतंकवादी कहता है। तुर्की लंबे समय से चाहता था कि अमरीका कुर्दों के साथ सहयोग बंद करे।
कुर्दिश लड़ाका सीरियाई डेमोक्रेटिक फ़ोर्सेज यानी एसडीएफ़ के हिस्सा रहे हैं और यह धड़ा सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ अमरीका का सबसे विश्वसनीय साथी रहा है।
अमरीका के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन से सीधे बात की है। तुर्की सीरिया में कुर्दों के ख़िलाफ़ सैन्य ऑपरेशन चला सकता है लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इसका दायरा कितना बड़ा होगा।
अगर तुर्की की सेना अमरीका समर्थित कुर्दों से टकराती है तो इस इलाक़े में काफ़ी उलट-पुलट हो सकता है।
पिछले साल दिसंबर में ट्रंप ने सीरिया से अपने सैनिको को बुलाने की घोषणा की थी लेकिन देश के भीतर विरोध के बाद पीछे हटना पड़ा था। ट्रंप के इस फ़ैसले से अमरीका के यूरोप के सहयोगी भी ख़ुश नहीं थे।
वॉशिंगटन इंस्टिट्यूट में टर्किश रिसर्च प्रोग्राम के निदेशक सोनेर कैगप्टे 'अर्दोआन्स एम्पायर: टर्की एंड द पॉलिटिक्स ऑफ़ मिडल ईस्ट' किताब के लेखक हैं।
उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से टेलिफ़ोन इंटरव्यू में कहा है, ''अमरीका के विरोध के बिना तुर्की उत्तरी सीरिया में हमला कर कुर्दिश नियंत्रण वाले सीरियाई इलाक़े में अपनी मौजूदगी बना लेगा। ऐसे में अर्दोआन यहां हजारों सीरियाई शरणार्थियों को भेज सकते हैं और वो दावा करेंगे कि सीरिया में ट्रंप की नीतियों में उनका भी दख़ल है। यह एक अहम प्रगति है।''
ये आशंका भी जताई जा रही है कि इसकी आड़ में तुर्की वहां पर मौजूद कुर्द लड़ाकों पर हमले कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने धमकी दी है कि तुर्की ऐसा करेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था को वो तबाह कर देंगे।
व्हाइट हाउस ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की की सेना को सीरिया से लगी सीमा में सीमित ऑपरेशन की अनुमति दे दी है। अमरीका ने कहा है कि तुर्की के इस ऑपरेशन से अमरीका समर्थित कुर्द बल अलग रहेंगे। सीरियाई विशेषज्ञ व्हाइट हाउस के इस फ़ैसले की आलोचना कर रहे हैं।
इनका कहना है कि अमरीका का कुर्दों को छोड़ देने से आठ सालों से जारी सीरियाई संकट का दायरा और बढ़ सकता है। ये भी संभव है कि कुर्द सीरियाई सरकार बशर अल-असद के साथ आ सकते हैं। बशर अल-असद की सेना तुर्की से लड़ने के लिए तैयार बैठी है।
अरिज़ोना के डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव और इराक़ युद्ध में नौसेना के हिस्सा रहे रुबेन गैलेगो ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तरी सीरिया में तुर्की की दस्तक मध्य-पूर्व को अस्थिर करने वाला क़दम साबित होगा।
उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''इसके बाद कुर्द अमरीका पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। वे नए सहयोगी की ओर देखेंगे ताकि वो अपनी आज़ादी और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें।''
अमरीका की यह घोषणा एसडीएफ़ के लिए चौंकाने वाली है। एसडीएफ़ की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका के इस फ़ैसले से इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ाई और शांति को झटका लगेगा।
तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन पूर्व में तुर्की-सीरियाई सीमा से 300 मील तक सेफ़ ज़ोन की मांग कर रहे हैं। वो इस इलाक़े को 10 लाख सीरियाई शरणार्थियों के लिए चाहते हैं।
ये शरणार्थी अभी तुर्की में हैं। अर्दोआन ने धमकी दे रखी है अगर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला तो वो इन शरणार्थियों को यूरोप में भेजना शुरू कर देंगे। अर्दोआन चाहते हैं कि सीरियाई शरणार्थी अब वापस जाएं।
अगस्त महीने की शुरुआत से अमरीकी और तुर्की सेना साथ मिलकर काम कर रही है। ये 300 मील लंबे सीमाई इलाक़े के 75 मील क्षेत्र में साथ में गश्ती लगाने का काम भी कर रहे थे।
अमरीका समर्थित कुर्द बल कई मील पीछे गए और अपने क़िलेबंदी को भी नष्ट किया। अर्दोआन के लिए यह प्रगति अब भी नाकाफ़ी है। पिछले हफ़्ते ही उन्होंने संकेत दिए थे कि सीमाई इलाक़े में तुर्की हमला कर सकता है।
अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि टर्किश बॉर्डर अमरीकन फ़ोर्स को इस ऑपरेशन में अमरीका की ओर से क्या मदद मिलेगी? न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार उत्तरी सीरिया में अमरीका के एक हज़ार सैनिक हैं और इनके साथ कुल 60 हज़ार कुर्द लड़ाके हैं।
कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमरीका सीरिया से बाहर होकर फिर जगह नहीं बना पाएगा। तुर्की नेटो का बड़ा सदस्य देश है लेकिन कुर्द इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ अमरीका की लड़ाई के पार्टनर रहे हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स से एक अमरीकी अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, ''हमलोग न तो तुर्क का समर्थन करने जा रहे और न ही एसडीएफ़ का। अगर ये आपस में लड़ेंगे तो हमलोग बिल्कुल अलग रहेंगे।''
दिसंबर 2018 में अमरीका के विदेश मंत्री जिम मैटिस ने सीरिया से सभी 2000 सैनिकों की वापसी के आदेश को लेकर इस्तीफ़ा दे दिया था।
हालांकि तुर्की पूरे मामले को बिल्कुल अलग तरीक़े से देख रहा है। तुर्की में यह समझ है कि इस मसले पर राष्ट्रपति ट्रंप और सेना के अधिकारियों में सहमति नहीं है।
अर्दोआन सीरिया को लेकर अमरीका भी गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आयोजित ग्रुप डिनर पार्टी में अर्दोआन शामिल हुए थे। ट्रंप ने कहा था कि अर्दोआन उनके दोस्त बन गए हैं। हालांकि दोनों के बीच प्राइवेट मीटिंग नहीं हो पाई थी।
एक समय उस्मानी साम्राज्य के केंद्र रहे तुर्की में कुर्दों की आबादी 20 फ़ीसदी है। कुर्द संगठन आरोप लगाते हैं कि उनकी संस्कृति पहचान को तुर्की में दबाया जा रहा है। ऐसे में कुछ संगठन 1980 के दशक से ही छापामार संघर्ष कर रहे हैं।
अमरीका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर मुक़्तदर ख़ान कहते हैं कि इस मामले को समझने के लिए इतिहास में जाना होगा।
वह बताते हैं, "तुर्की में दो नस्लीय पहचानें हैं- तुर्क और कुर्द. कुर्द आबादी लगभग 20 प्रतिशत है। पहले वे सांस्कृतिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे मगर अब कई सालों से वे आज़ादी की मांग कर रहे हैं। वे कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं।''
मध्य-पूर्व के नक्शे में नज़र डालें तो तुर्की के दक्षिण-पूर्व, सीरिया के उत्तर-पूर्व, इराक़ के उत्तर-पश्चिम और ईरान के उत्तर- पश्चिम में ऐसा हिस्सा है, जहां कुर्द बसते हैं।
कुर्द हैं तो सुन्नी मुस्लिम, मगर उनकी भाषा और संस्कृति अलग है। प्रोफ़ेसर मुक़्तरदर ख़ान बताते हैं कि कुर्द मांग करते है कि संयुक्त राष्ट्र के आत्मनिर्णय के अधिकार पर उन्हें भी अलग कुर्दिस्तान बनाने का हक़ मिले। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमरीका ने 2003 में इराक़ पर हमला किया था। तभी से उत्तरी इराक़ में कुर्दिस्तान लगभग स्वतंत्र राष्ट्र की तरह काम कर रहा है।
अमरीका के डेलेवेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर मुक़्तदर ख़ान कहते हैं, "तुर्की इस बात से डरा हुआ है कि कुर्दों का एक राष्ट्र सा लगभग बना हुआ है, ऊपर से कुर्द लड़ाकों को आईएस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अमरीका से हथियार भी मिले हैं। ऐसा भी सकता है कि कुर्द इतने शक्तिशाली हो जाएं कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट से जीते हुए हिस्से को इराक़ के कुर्दिस्तान से जोड़कर बड़ा सा कुर्द राष्ट्र बना लें। ऐसा हुआ तो तुर्की के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा।''
तुर्की को यह चिंता पहले भी थी। शुरू में जब आईएस के ख़िलाफ़ अमरीका ने क़ुर्दों से सहयोग लेना चाहा था, तब भी तुर्की ने इसका विरोध किया था। ऐसे में यह आशंका बनी हुई है कि जैसे ही अमरीका सीरिया से अपनी सेनाएं हटाएगा, तुर्की वहां पर कार्रवाई करके कुर्द इलाक़ों को ख़त्म कर देगा और उनके नियंत्रण वाली ज़मीन छीन लेगा।