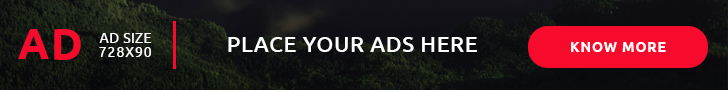एक अहम फ़ैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2020 को दिए आदेश में कहा है कि अपनी पसंद के शख़्स के साथ रहने का अधिकार, चाहे उनका मज़हब कुछ भी हो, जीवन और निजी आज़ादी के अधिकार का स्वाभाविक तत्व है।
आदेश को आए 15 दिन हो गए हैं लेकिन इसकी प्रति इसी हफ़्ते उपलब्ध हुई है जिसके बाद इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज नक़वी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने यह अहम फ़ैसला सुनाया है।
प्रियांशी उर्फ़ समरीन और अन्य, बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य में दिए गए आदेश और इसके बाद आए नूर जहां बेगम उर्फ़ अंजली मिश्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में दिए गए आदेशों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, ''इनमें से किसी भी आदेश में दो परिपक्व लोगों के अपना साथी चुनने की आज़ादी के अधिकार को नहीं देखा गया है।"
कोर्ट ने आदेश दिया, ''नूर जहां और प्रियांशी के मामलों में दिए गए फ़ैसलों को हम अच्छा क़ानून नहीं मानते हैं।''
आइए नज़र डालते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या अहम बातें कहीं हैं ...
- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, ''हम प्रियंका खरवार और सलामत को हिंदू और मुस्लिम के तौर पर नहीं देखते हैं। इसके बजाय हम इन्हें दो वयस्क लोगों के रूप में देखते हैं जो अपनी इच्छा और चुनाव से शांतिपूर्वक और ख़ुशी से एक साथ रह रहे हैं।''
- "अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, जीवन और निजी आज़ादी के अधिकार में निहित है। निजी संबंधों में दख़ल दो लोगों के चुनाव करने की आज़ादी में गंभीर अतिक्रमण होगा।''
- कोर्ट ने कहा है, "वयस्क हो चुके शख़्स का अपनी पसंद के शख़्स के साथ रहने का फ़ैसला किसी व्यक्ति के अधिकार से जुड़ा है और जब इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह उस शख़्स के जीवन जीने और निजी आज़ादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि इसमें चुनाव की आज़ादी, साथी चुनने और सम्मान के साथ जीने के संविधान के आर्टिकल-21 के सिद्धांत शामिल हैं।''
- कोर्ट ने अपने फ़ैसले में शफ़ीन जहां बनाम अशोकन केएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का ज़िक्र किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार एक वयस्क हो चुके व्यक्ति की आज़ादी का सम्मान किया है।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शक्ति वाहिनी बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का भी ज़िक्र किया। इसके अलावा कोर्ट ने नंद कुमार बनाम केरल सरकार में आए फ़ैसले का भी हवाला दिया और कहा कि इन फ़ैसलों में साफ़ है कि वयस्क हो चुके शख़्स के पास अपना चुनाव करने की आज़ादी है।
- कोर्ट ने निजता के अधिकार को लेकर के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का भी ज़िक्र किया और कहा कि साथी चुनने के अधिकार का जाति, पंथ या मज़हब से कोई लेना-देना नहीं है और यह आर्टिकल-21 के अभिन्न हिस्से जीवन जीने और निजी स्वतंत्रता में निहित है।
- नूरजहां और ऐसे ही दूसरे मामलों में आए फ़ैसलों पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि वयस्क हो चुके शख़्स की मर्ज़ी को अनदेखा करना न केवल चुनाव की आज़ादी के विपरीत होगा बल्कि यह विविधता में एकता के सिद्धांत के लिए भी ख़तरा होगा।
- प्रियांशी और नूरजहां मामलों में आए फ़ैसलों पर कोर्ट ने कहा कि इनमें से किसी भी फ़ैसले में दो परिपक्व लोगों के अपना साथी चुनने या उन्हें किसके साथ रहना है। इसका चुनाव करने की आज़ादी के जीवन और आज़ादी से जुड़े मसले को ध्यान में नहीं रखा गया है। कोर्ट ने आगे कहा है कि नूर जहां और प्रियांशी मामलों में आए फ़ैसले क़ानून के लिहाज़ से अच्छे नहीं हैं।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज नक़वी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने अपने इसी आदेश में टिप्पणी की है, "हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर क़ानून दो समलैंगिक लोगों को शांतिपूर्वक एक साथ रहने की इजाज़त देता है तो न तो किसी शख़्स न ही किसी परिवार या यहां तक कि राज्य को भी दो वयस्क लोगों को अपनी इच्छा से एक साथ रहने पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है।''
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला और पृष्ठभूमि
इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडवोकेट अरविंद कुमार त्रिपाठी कहते हैं, ''इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया जजमेंट में जो एफ़आईआर ख़ारिज की गई है वह इस बात पर आधारित है कि क्या दो वयस्क लोग आर्टिकल-21 के तहत एक साथ रह सकते हैं या नहीं?"
त्रिपाठी कहते हैं कि ''जहां तक शादी की बात है तो शादी का धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध इच्छा से है। और इच्छा का संबंध आर्टिकल-21 की लिबर्टी से है। ऐसे में पहले के फ़ैसलों के मुक़ाबले इस फ़ैसले में ज़्यादा स्पष्टता है।''
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाश्वत आनंद कहते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला बहुत अच्छा है और इसमें निजता की स्वतंत्रता और इच्छा की स्वतंत्रता को आधार बनाया गया है।
इस मामले की पृष्ठभूमि यह है कि सलामत अंसारी और तीन अन्य की तरफ़ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाख़िल की गई थी। सलामत अंसारी और उनकी पत्नी प्रियंका खरवार उर्फ़ आलिया ने दो अन्य लोगों के साथ हाईकोर्ट में उनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर को ख़ारिज करने की माँग की थी।
इस मामले में प्रियंका धर्म परिवर्तन कर आलिया बन गई थीं और और उन्होंने सलामत अंसारी से निकाह कर लिया था। इसके विरोध में प्रियंका के पिता ने एफ़आईआर दर्ज करा दी थी। इस एफ़आईआर में 363, 366, 352 समेत पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 भी लगाई गई थीं। इसमें सलामत, उनके भाई और उनकी मां को आरोपी बनाया गया था।
कोर्ट ने प्रियंका उर्फ़ आलिया की जन्मतिथि देखी और पाया गया कि वो वयस्क हैं। आनंद कहते हैं कि ऐसे में पॉक्सो के सारे एक्ट ख़ारिज हो गए। साथ ही ज़ोर-ज़बरदस्ती वाली धाराओं को कोर्ट ने माना कि इन्हें फँसाने के लिए लगाया गया है।
सलामत अंसारी की ओर से हाईकोर्ट में तर्क दिया गया था कि सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार उर्फ़ आलिया वयस्क हैं और शादी करने के लिए योग्य हैं। इस पक्ष ने कहा कि प्रियंका के अपनी हिंदू पहचान को छोड़ने और इस्लाम अपनाने के बाद इन दोनों ने 19.8.2019 को मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह कर लिया था।
दोनों लोग बीते एक साल से बतौर पति-पत्नी साथ रह रहे हैं। दोनों ने कहा कि प्रियंका के पिता ने ग़लत मक़सद से उनके विवाह को ख़त्म करने के लिए यह एफ़आईआर दर्ज कराई है और चूंकि इन दोनों ने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे में यह एफ़आईआर ख़ारिज की जानी चाहिए।
दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि शादी के मक़सद से किया गया धर्म परिवर्तन निषिद्ध है और इस तरह से हुई शादी की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। ऐसे में कोर्ट को इन लोगों को किसी तरह की राहत नहीं देनी चाहिए।
आनंद कहते हैं कि सरकार ने पिछले दो फ़ैसलों के आधार पर सलामत को राहत न देने की माँग की थी। आनंद कहते हैं, ''कोर्ट ने कहा कि जब इन दो वयस्क लोगों ने साथ रहने का तय कर लिया तो हमें आर्टिकल-21 का आदर करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस एफ़आईआर को ख़ारिज कर दिया।''
नूरजहां और प्रियांशी के मामले
सितंबर 2020 में प्रियांशी के मामले में सिंगल बेंच ने 2014 में नूरजहां बेगम उर्फ़ अंजली मिश्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले का ज़िक्र किया था जिसमें कहा गया था कि महज़ शादी के मक़सद से किया गया धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य है।
नूरजहां बेगम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादीशुदा जोड़े के तौर पर सुरक्षा की दरकार के लिए दायर की गई याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया था। इस मामले में भी लड़की ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था और इसके बाद निकाह कर लिया था।
इसी तरह के चार अन्य मामले भी कोर्ट के सामने आए थे।
इन मामलों में महिलाएं अपने कथित धर्म परिवर्तन को प्रमाणित नहीं कर पाई थीं क्योंकि वे इस्लाम की समझ को साबित करने में नाकाम रही थीं। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये कथित शादी अवैध हैं क्योंकि इसे एक ऐसे धर्म परिवर्तन के बाद किया गया था जिसे क़ानून के मुताबिक़ जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है।
आनंद कहते हैं, ''लेकिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने इस फ़ैसले में कहा है कि जब एक बार यह साबित हो गया था कि शादी करने वाले दोनों लोग वयस्क हैं तो कोर्ट को इनके मज़हब पर जाना ही नहीं चाहिए था।''
हालिया फ़ैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में ऐसे ही पिछले मामलों में आए फ़ैसलों का ज़िक्र किया है।
योगी सरकार का जबरन धर्मांतरण रोकने का अध्यादेश
हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 नवंबर 2020 को 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020' को मंज़ूरी दे दी है।
इस क़ानून के अनुसार 'जबरन धर्मांतरण' उत्तर प्रदेश में दंडनीय होगा। इसमें एक साल से 10 साल तक जेल हो सकती है और 15 हज़ार से 50 हज़ार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
योगी सरकार के इस अध्यादेश के अनुसार 'अवैध धर्मांतरण' अगर किसी नाबालिग़ या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं के साथ होता है तो तीन से 10 साल की क़ैद और 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता विनोद मिश्रा कहते हैं, "सरकार ने इस क़ानून के ज़रिए जबरन धर्मांतरण या दूसरी ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की है। सरकार कथित 'लव जिहाद' पर लगाम लगाना चाहती है।"
क्या टकराव पैदा होगा?
क्या उत्तर प्रदेश सरकार के लाए गए 'अवैध धर्मांतरण' रोकने के क़ानून और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले के बीच आने वाले दिनों में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है?
इस मसले पर हाईकोर्ट में एडवोकेट अरविंद कुमार त्रिपाठी कहते हैं, "अभी ये कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि सरकार ने जो अध्यादेश पास किया है जो अभी न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बना है। जब तक इस पर केस फ़ाइल नहीं होता तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि ये दोनों फ़ैसले एक-दूसरे से टकरा सकते हैं या नहीं।"
त्रिपाठी कहते हैं, "दिलचस्प बात यह है कि जिस कथित लव जिहाद को लेकर माहौल बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अध्यादेश को पेश किया है वह ज्यूडिशियल रिव्यू में टिक नहीं पाएगा. लेकिन, जब इसे चैलेंज किया जाएगा तब स्थिति साफ़ होगी।"
सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शाश्वत आनंद कहते हैं कि योगी सरकार का लाया गया क़ानून दरअसल ज़बरदस्ती होने वाले धर्मांतरण पर है और इसे 'लव जिहाद' का क़ानून कहना सही नहीं होगा।
वह कहते हैं, "उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश ज़बरदस्ती होने वाले धर्म-परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। अब अगर कभी इस क़ानून का दुरुपयोग होता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फ़ैसला एक दीवार बनकर काम करेगा।"
वह कहते हैं कि इस तरह के मामलों में एक पक्ष कहेगा कि यह जबरन धर्मांतरण है जबकि दूसरा पक्ष इसे सहमति से बताएगा। ऐसे में योगी सरकार के क़ानून के ग़लत इस्तेमाल पर हाईकोर्ट का फ़ैसला ढाल का काम करेगा।
आने वाले वक़्त में यह साफ़ हो सकेगा कि योगी सरकार के लाए गए अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला कैसे प्रभावित करेगा?